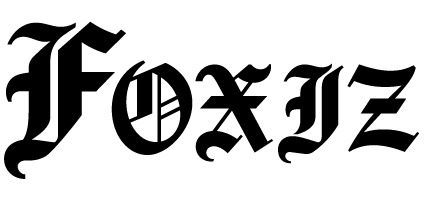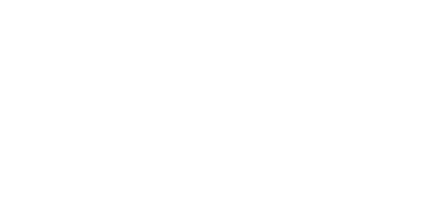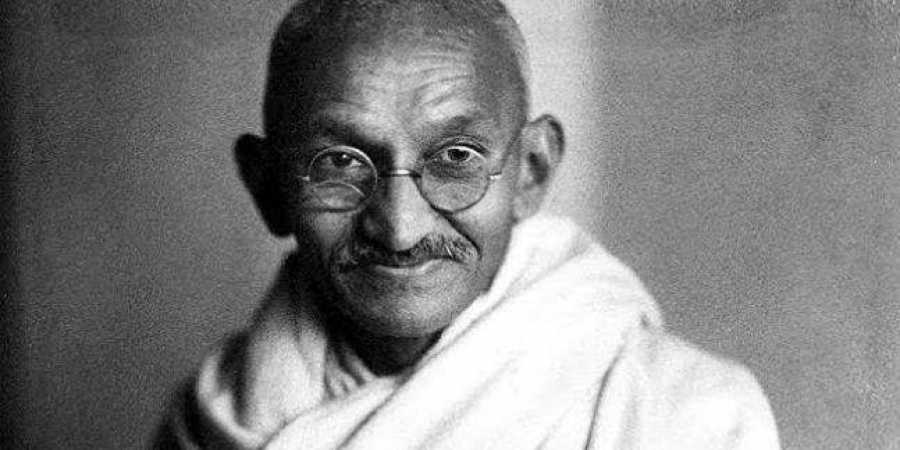महात्मा गांधी के एक सहयोगी ने एक बार बताया था कि 1918 में उन्हें फ्लू हो गया था। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए उन्हें चार साल गुजर गए थे।
अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, गुजरात के उनके आश्रम में स्पेनिश फ्लू हो गया था। उस वक्त महात्मा गांधी की उम्र 48 साल थी।
फ्लू के दौरान उन्हें पूरी तरह से आराम करने को कहा गया था। वो सिर्फ तरल पदार्थों का सेवन कर रहे थे। वो पहली बार इतने लंबे दिनों के लिए बीमार हुए थे।
जब उनकी बीमारी की खबर फैली तो एक स्थानीय अखबार ने लिखा था, ‘गांधीजी की जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि देश की है।’
यह फ्लू बॉम्बे (अब मुंबई) में एक लौटे हुए सैनिकों के जहाज से 1918 में पूरे देश में फैला था। हेल्थ इंस्पेक्टर जेएस टर्नर के मुताबिक इस फ्लू का वायरस दबे पांव किसी चोर की तरह दाखिल हुआ था और तेजी से फैल गया था। उसी साल सितंबर में यह महामारी दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में फैलनी शुरू हुई।
इंफ्लुएंजा की वजह से करीब पौने दो करोड़ भारतीयों की मौत हुई है जो विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की तुलना में ज्यादा है। उस वक्त भारत ने अपनी आबादी का छह फीसदी हिस्सा इस बीमारी में खो दिया। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं।
ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि महिलाएं बड़े पैमाने पर कुपोषण का शिकार थीं। वो अपेक्षाकृत अधिक अस्वास्थ्यकर माहौल में रहने को मजबूर थीं। इसके अलावा नर्सिंग के काम में भी वो सक्रिय थीं।
ऐसा माना जाता है कि इस महामारी से दुनिया की एक तिहाई आबादी प्रभावित हुई थी और करीब पांच से दस करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। गांधी और उनके सहयोगी किस्मत के धनी थे कि वो सब बच गए।
हिंदी के मशूहर लेखक और कवि सुर्यकांत त्रिपाठी निराला की बीवी और घर के कई दूसरे सदस्य इस बीमारी की भेंट चढ़ गए थे। वो लिखते हैं, ‘मेरा परिवार पलक झपकते ही मेरे आंखों से ओझल हो गया था।’
ये हालात और खराब हो गए जब खराब मानसून की वजह से सुखा पड़ गया और आकाल जैसी स्थिति बन गई। इसकी वजह से लोग और कमजोर होने लगे। उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। शहरों में भीड़ बढ़ने लगी। इससे बीमार पड़ने वालों की संख्या और बढ़ गई।
उस वक्त मौजूद चिकित्सकीय व्यवस्थाएं आज की तुलना में और भी कमतर थीं। हालांकि इलाज तो आज भी कोरोना का नहीं है लेकिन वैज्ञानिक कम से कम कोरोना वायरस की जीन मैपिंग करने में कामयाब जरूर हो पाए हैं।
इस आधार पर वैज्ञानिकों ने टीका बनाने का वादा भी किया है। 1918 में जब फ्लू फैला था तब एंटीबायोटिक का चलन इतने बड़े पैमाने पर नहीं शुरू हुआ था। इतने सारे मेडिकल उपकरण भी मौजूद नहीं थे जो गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज कर सके।
पश्चिमी दवाओं के प्रति भी देश में एक स्वीकार का भाव नहीं था और ज्यादातर लोग देसी इलाज पर ही
यकीन करते थे। लेकिन इन दोनों ही महामारियों के फैलने के बीच भले ही एक सदी का फासला हो लेकिन इन दोनों के बीच कई समानताएं दिखती हैं। संभव है कि हम बहुत सारी जरूरी चीजें उस फ्लू के अनुभव से सीख सकते हैं।
बॉम्बे जैसे बड़ी आबादी वाले शहर में संक्रमण फैलने के कारण तेजी से फ्लू का प्रकोप फैला था इसलिए वैज्ञानिक मौजूदा चुनौती को लेकर डरे हुए हैं।
मुंबई की मौजूदा आबादी दो करोड़ से ज्यादा है। यह देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। महाराष्ट्र से, जहां की राजधानी मुंबई है, सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं।
साल 1918 की जुलाई में हर रोज करीब 230 लोग फ्लू की वजह से मारे जा रहे थे। यह जून में हर रोज मरने वालों से तीन गुना अधिक संख्या थी।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी के मुख्य लक्षण है कम से कम तीन दिन से तेज बुखार और पीठ में दर्द होना। अखबार ने अपनी रिपोर्टिंग में आगे लिखा है, ‘बॉम्बे में करीब हर घर में किसी न किसी को बुखार की शिकायत है।
इसका सबसे अच्छा उपचार है कि चिंता न करे और आराम करे। मत भूलें कि कोरोना मुख्य तौर पर संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से होता है।’
अखबार ने लोगों को सलाह दी है कि वे दफ्तरों और फैक्ट्रियों से दूर अपने-अपने घरों में रहे और बाहर ना निकलें। इसके अलावा भीड़-भाड़ वाली जगह मसलन मेला, त्यौहार, थिएटर, स्कूल, सिनेमा घर, रेलवे प्लेटफॉर्म या फिर लेक्चर हॉल जैसी जगहों पर जाने से बचे।
इसके अलावा हवादार घर में सोने, पोषक खाना खाने और कसरत करने की सलाह दी गई है। इन सबसे ज्यादा अहम सलाह जो अखबार ने दी है, वो है इस बीमारी के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होना।
औपनिवेशिक काल के अधिकारी इस बात को लेकर अलग राय रखते हैं कि 1918 में यह फ्लू कैसे फैला था। हेल्थ इंस्पेक्टर टर्नर जहां यह मानते थे कि बॉम्बे के बंदरगाह पर बाहर से आए जहाज ने यह बीमारी लाई तो वहीं सरकार का मानना था कि यह फ्लू शहर में कहीं बाहर से नहीं आया था, बल्कि यहीं फैला था।
उस वक्त महामारी के चपेट में आए बॉम्बे शहर ने इससे कैसे मुकाबला किया, इस विषय पर इतिहासकार मृदुला रमन्ना ने काम किया है।
वो बताती हैं, ‘जिन महामारियों को भारत में नियंत्रित करने में औपनिवेशिक काल के अधिकारी नाकामयाब रहते थे, उसके प्रसार के लिए वो भारत की गंदगी को जिम्मेवार ठहरा देते थे।’
बाद में सरकार की एक रिपोर्ट में इस पर नाराजगी जाहिर की गई और इसे सुधारने पर जोर दिया गया। अखबारों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की शिकायत की कि आपातकालीन स्थिति में सरकारी अधिकारी पहाड़ों में चले जाते हैं और लोगों को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं।
लॉरा स्पिनी ने पेल राइडर- द स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918 नाम की किताब लिखी है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे अस्पताल के सफाईकर्मियों को इलाज करा रहे ब्रितानी सैनिकों से दूर रखा गया था।
ये सफाईकर्मी उस वक्त को याद करते हैं जब 1886 से 1914 के बीच अस्सी लाख लोग मारे गए थे। लॉरा स्पिनी लिखती हैं, ‘औपनिवेशिक अधिकारियों को स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को अनदेखी करनी की कीमत चुकानी पड़ी थी।
हालांकि यह भी सच है कि वे ऐसी त्रासदी का मुकाबला करने में सक्षम बहुत सक्षम नहीं थे। डॉक्टरों की भी भारी कमी थी क्योंकि वे जंग के मैदान में तैनात थे।’
आखिरकार गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सेवी समूहों ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला था। उन्होंने छोटे-छोटे समूहों में कैंप बना कर लोगों की सहायता करनी शुरू की। पैसे इकट्ठा किए, कपड़े और दवाइयां बांटी।
नागरिक समूहों ने मिलकर कमिटियां बनाईं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, ‘भारत के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ था जब पढ़े-लिखे लोग और समृद्ध तबके के लोग गरीबों की मदद करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सामने आए थे।’
आज की तारीख में जब फिर एक बार ऐसी ही एक मुसीबत सामने मुंह खोले खड़ी है तब सरकार चुस्ती के साथ इसकी रोकथाम में लगी हुई है लेकिन एक सदी पहले जब ऐसी ही मुसीबत सामने आई थी तब नागरिक समाज ने बड़ी भूमिका निभाई थी। जैसे-जैसे कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पहलू को भी हमें ध्यान में रखना होगा।